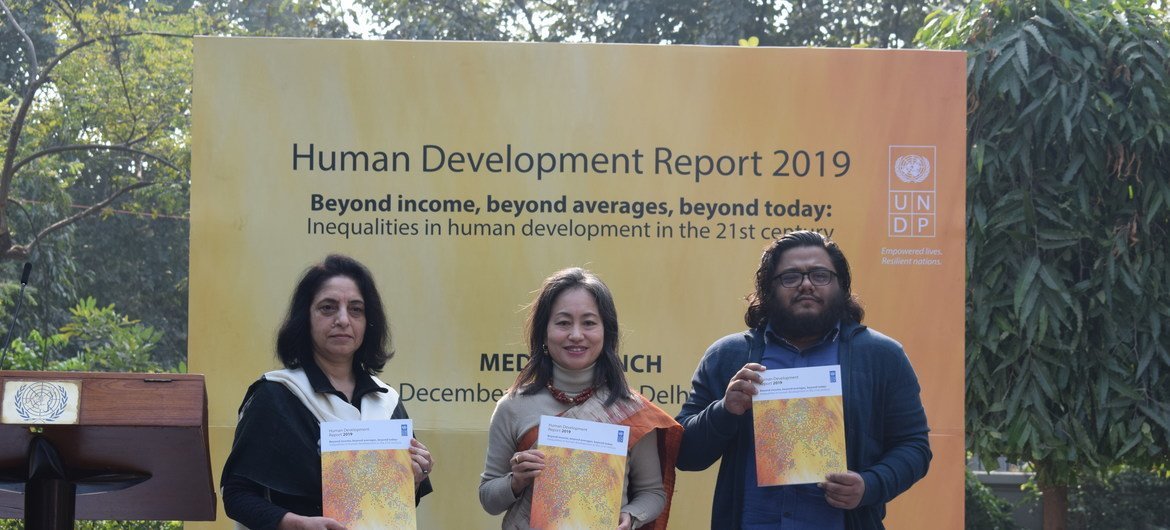प्रगति की राह पर दक्षिण एशिया लेकिन चुनौतियां बरक़रार
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की नई रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया ने मानव विकास के क्षेत्र में सबसे तेज़ प्रगति हासिल की है. वर्ष 1990 से 2018 की अवधि में दक्षिण एशिया क्षेत्र में 46 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जिसके बाद 43 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र का स्थान है. लेकिन दक्षिण एशिया में ही बहुआयामी ग़रीबी से पीड़ित लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या भी रहती है है और जलवायु परिवर्तन हालात को और ज़्यादा गंभीर बना रही है.
2019 मानव विकास सूचकांक के आधार पर 189 देशों में भारत 129वें स्थान पर है जबकि पिछले वर्ष उसकी रैंकिंग 130 थी. रिपोर्ट बताती है कि जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में बेहतरी के साथ-साथ पूर्ण ग़रीबी में गिरावट के कारण हालात बेहतर हो रहे हैं.
भारत का एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक 50 प्रतिशत (0.431 से 0.647 तक) बढ़ा है, जो इसे मध्यम मानव विकास समूह (0.634) के देशों में औसत से ऊपर और अन्य दक्षिण एशियाई देशों (0.642) में भी औसत से ऊपर रखता है.
इसके अलावा इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों देश उच्च मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं.
दक्षिण एशिया में जीवन प्रत्याशा और स्कूली शिक्षा में सबसे अधिक प्रगति देखने को मिली है.
भारत के संदर्भ में वर्ष 1990 और 2018 के बीच जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.6 वर्षों की वृद्धि हुई, स्कूली शिक्षा में 3.5 वर्षों की वृद्धि हुई और संभावित स्कूली शिक्षा में 4.7 वर्ष की वृद्धि हुई.
प्रति व्यक्ति आय में 250 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई लेकिन बुनियादी मानकों और क्षमताओं में सुधार से हटकर देखने पर तस्वीर जटिल हो जाती है.
भारत में यूएनडीपी की प्रतिनिधि शोको नाडा ने सोमवार को ये रिपोर्ट जारी होने के मौक़े पर कहा, “पूर्ण ग़रीबी को कम करने में बड़ी कामयाबी दिखाने वाले भारत जैसे देशों के लिए हम आशा करते हैं कि 2019 मानव विकास रिपोर्ट उन असमानताओं और अभावों की ओर ध्यान दिलाएगी जो आय से परे हैं.”

ये क्षेत्र तकनीकी परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं. वर्ष 1987 से 2007 तक स्थापित बैंडविड्थ क्षमता की वैश्विक रैंकिंग में थोड़ा ही बदलाव देखने को मिला था लेकिन नई सदी में पूर्वी और उत्तरी एशिया में बैंडविड्थ के विस्तार के साथ परिवर्तन शुरू हो गया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया में स्थापित बैंडविड्थ क्षमता में चीन सबसे आगे है और स्थापित बैंडविड्थ की संभावना के मामले में भारत का हिस्सा जर्मनी, ब्राज़ील और फ्रांस के बराबर है.
प्रगति की राह में चुनौतियां
लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक के बाद तृतीयक (टर्शियरी) शिक्षा की दर धनी देशों के मुक़ाबले काफ़ी पिछड़ी हुई है.
भारत में तृतीयक श्रेणी शिक्षा प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत 24.5 और पूर्वी एशिया व प्रशांत क्षेत्र में 44 फ़ीसदी है.
पूरे क्षेत्र में लाखों-करोड़ों लोगों को बहुआयामी ग़रीबी के क़हर से बाहर निकाला गया है लेकिन इसमें सबसे अधिक प्रगति भारत में देखने को मिली है.
वर्ष 2005-06 से 2015-16 की अवधि में 27 करोड़ 10 लाख लोग ग़रीबी से बाहर निकाले गए हैं.
बहुआयामी ग़रीबी का सभी देशों में अलग रूप देखने को मिलता है. विश्व में 1 अरब 30 करोड़ बहुआयामी ग़रीबों में से 66 करोड़ से ज़्यादा लोग एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं.
यह दुनिया के 101 देशों में रहने वाले बहुआयामी ग़रीबी से पीड़ितों की लगभग आधी संख्या है.
केवल दक्षिण एशिया में बहुआयामी ग़रीबों की कुल संख्या का 41 प्रतिशत लोग रहते हैं जबकि भारत में कुल संख्या का 28 फ़ीसदी बसते हैं.
दक्षिण एशिया में हर दस में से चार लोगों के पास अब भी स्वच्छता सुविधाओं की कमी है.
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सबसे ग़रीब समुदाय जलवायु परिवर्तन से उपजते ख़तरों का सामना कर रहे हैं.
वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर एशिया के कई देशों में ग़रीबों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा. ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाले ग़रीब और कमज़ोर वर्ग को दोहरा आघात लगने की आशंका है: वैश्विक पैदावार में गिरावट से खाद्य क़ीमतों में बढ़ोत्तरी और आजीविका के साधनों पर नकारात्मक असर.
लैंगिक पूर्वाग्रहों से प्रगति में बाधा
रिपोर्ट बताती है कि प्रगति के बावजूद भारतीय उपमहाद्वीप पर समूह आधारित असमानताएं बनी हुई हैं जिनसे महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से प्रभावित हो रही हैं.
मानव विकास सूचकांक में दक्षिण एशिया और दूसरे क्षेत्रों में काफ़ी अंतर नज़र आता है. पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र लैंगिक विकास सूचकांक के मामले में दूसरे स्थान पर है, वहीं कोरिया गणराज्य लैंगिक असमानता सूचकांक में सबसे आगे है.
रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर में महिलाओं के ख़िलाफ़ अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की सबसे कम घटनाएं दर्ज की गई हैं.
वहीं दक्षिण एशिया की 31 प्रतिशत महिलाओं ने अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का अनुभव किया है.
जैंडर डवेलपमेंट इंडेक्स (0.829 बनाम 0.828) पर भारत, दक्षिण एशियाई औसत से थोड़ा ही बेहतर है और 2018 जेंडर असमानता सूचकांक पर 162 देशों की सूची में 122वें स्थान पर है.